Description
Lo que aprenderás
-
भारत के नए श्रम संहिताओं को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
-
चार नई श्रम संहिताएँ कौन सी हैं और उनमें से कौन सी पहले ही अधिसूचित हो चुकी है?
-
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता के मुख्य उद्देश्य और प्रावधान क्या हैं?
-
औद्योगिक संबंध संहिता में औद्योगिक विवादों के समाधान और रोजगार की शर्तों के लिए क्या प्रमुख प्रावधान हैं?
-
भारतीय संविधान के कौन से भाग श्रम कानूनों और श्रमिकों के कल्याण के लिए आधार प्रदान करते हैं?
-
नए श्रम संहिताएँ मौजूदा कानूनों से कैसे भिन्न हैं, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में?
भारत के नए श्रम कानून: एक विस्तृत अध्ययन मार्गदर्शिका
I. पृष्ठभूमि और उद्देश्य
ऐतिहासिक संदर्भ: भारत में ब्रिटिश-युग के श्रम कानूनों का प्रभुत्व कैसे रहा है और स्वतंत्रता के बाद से इनमें बदलाव के प्रयास कैसे किए गए हैं?
वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण: श्रम कानूनों में ‘संपूर्ण निरसन’ की वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता क्या है और इसके पीछे क्या तर्क हैं (जैसे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’)?
श्रम सशक्तिकरण का महत्व: श्रमिकों के लिए श्रम सशक्तिकरण क्यों महत्वपूर्ण है?
नए कोड का प्राथमिक उद्देश्य: नए श्रम कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ‘आत्मनिर्भर’ शब्द के संदर्भ में इसके निहितार्थ क्या हैं?
त्रिपक्षीय प्रणाली: भारत में श्रम कल्याण के लिए नियोक्ता, कर्मचारी और सरकार की त्रिपक्षीय प्रणाली की भूमिका क्या है?
II. श्रम कानूनों का विकास और वर्तमान स्थिति
श्रम कानून का उद्देश्य: किसी भी श्रम कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल श्रमिक कल्याण या उद्योग के विकास पर केंद्रित रहा है?
उद्योग समर्थक झुकाव: स्वतंत्रता के बाद के अधिकांश कानून उद्योग के पक्ष में क्यों बनाए गए थे?
ट्रेड यूनियनें: ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत ट्रेड यूनियनों के गठन की स्वतंत्रता का क्या महत्व है? उनकी सामूहिक सौदेबाजी शक्ति की भूमिका क्या है?
‘हायर एंड फायर’ का नारा: नए कोड के संदर्भ में ‘हायर एंड फायर’ की अवधारणा को कैसे समझा जाता है?
1991 के बाद की मांग: 1991 में अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद उद्योग ने श्रम कानूनों में संशोधन की मांग क्यों की?
पुराने कानून: फैक्ट्री अधिनियम, 1948 जैसे कुछ पुराने कानूनों की निरंतर प्रासंगिकता क्या है?
III. संवैधानिक आधार और प्रशासनिक ढांचा
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के कौन से भाग (भाग III, भाग IV) श्रम कानूनों को जनादेश देते हैं?
मौलिक अधिकार: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 16, 19, 21, 23, 24) श्रम क्षेत्र को कैसे प्रभावित करते हैं?
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP): DPSP (जैसे काम का अधिकार, मानवीय कार्य की स्थिति, मातृत्व राहत, लिविंग वेज) श्रम विधानों को कैसे मार्गदर्शन करते हैं?
श्रम और रोजगार मंत्रालय: केंद्रीय सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय की भूमिका क्या है?
श्रम समवर्ती सूची में: ‘श्रम’ को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखने का क्या अर्थ है? केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिकाएँ क्या हैं?
सूचियाँ (केंद्रीय, समवर्ती): केंद्रीय और समवर्ती सूचियों में श्रम से संबंधित विशिष्ट प्रविष्टियों (जैसे खान, औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन, सामाजिक सुरक्षा) की पहचान करें।
कानूनों का प्रवर्तन: श्रम कानूनों के प्रवर्तन में केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न श्रेणियां और जिम्मेदारियां क्या हैं?
IV. चार नए श्रम कोड का विवरण
पुराने कानूनों का समेकन: कितने कानूनों को चार कोड में समेकित किया गया है? यह एक ‘पार्थ ब्रेकिंग’ पहल क्यों है?
सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण: नए कोड संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं?
इंस्पेक्टर राज का अंत: ‘इंस्पेक्टर राज’ प्रणाली को कैसे समाप्त किया गया है और श्रम निरीक्षकों की भूमिका कैसे बदली है?
असंगठित क्षेत्र पर ध्यान: सरकार असंगठित क्षेत्र (भारत के कार्यबल का 90% हिस्सा) के लिए क्या कर रही है?
प्रधान मंत्री के दर्शन: नए कोड प्रधान मंत्री के दर्शन (“न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन,” “आत्मनिर्भर भारत,” “सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास”) को कैसे दर्शाते हैं?
विवाद समाधान प्रणाली: नए कोड में विवाद समाधान प्रणाली पर क्या ध्यान दिया गया है?
V. विशिष्ट कोड
A. वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019)
समेकित कानून: इसने किन चार पुराने कानूनों को निरस्त किया है?
वेतन की परिभाषा: इस संहिता में वेतन की परिभाषा में क्या बदलाव आया है (शामिल और बहिष्कृत) और इसका क्या प्रभाव है (जैसे पीएफ योगदान)?
न्यूनतम मजदूरी का सार्वभौमीकरण: न्यूनतम मजदूरी को कैसे सार्वभौमिक बनाया गया है और क्षेत्रीय असमानता को कैसे दूर किया जाएगा (राष्ट्रीय फ्लोर वेज)?
न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा: न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा हर पाँच साल में क्यों की जाती है?
गुजरात मजदूर सभा मामला: गुजरात मजदूर सभा और अन्य बनाम गुजरात राज्य के मामले का क्या महत्व है? इसने श्रमिकों के अधिकारों को कैसे बरकरार रखा और महामारी के दौरान उनके शोषण को कैसे रोका?
संवैधानिक मूल्यों का समर्थन: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संवैधानिक मूल्यों (DPSP) को कैसे बरकरार रखा?
कार्यकर्ता और कर्मचारी की परिभाषा: ‘कार्यकर्ता’ और ‘कर्मचारी’ की परिभाषा में क्या अंतर है और इसका क्या निहितार्थ है?
B. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020)
समेकित कानून: इसने किन तीन कानूनों को निरस्त किया है?
नया कवरेज: पत्रकार और समाचार पत्र कर्मचारी तथा बिक्री संवर्धन कर्मचारी जैसे नए प्रवेशी इसमें कैसे शामिल हैं?
निश्चित अवधि रोजगार: निश्चित अवधि रोजगार को वैध बनाने का क्या महत्व है?
एकल वार्ताकार ट्रेड यूनियन: एक उद्योग के लिए एक एकल वार्ताकार ट्रेड यूनियन का प्रावधान क्या है और यह कैसे मदद करेगा?
शिकायत निवारण समितियां: शिकायत निवारण समितियों की भूमिका क्या है?
स्थायी आदेश: स्थायी आदेश किन उद्योगों के लिए अनिवार्य हैं (कार्यकर्ताओं की संख्या के संदर्भ में)?
हड़ताल और तालाबंदी के लिए नोटिस: हड़ताल और तालाबंदी के लिए अग्रिम सूचना की क्या आवश्यकताएँ हैं?
उपहार और अन्य लाभ: निश्चित अवधि रोजगार के लिए उपहार, ईएसआई, पीएफ, बोनस और अन्य लाभ कैसे प्रदान किए जाते हैं?
C. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code, 2020)
समेकित कानून: इसने किन नौ कानूनों को समेकित किया है?
नई परिभाषाएं: इस संहिता में किन नई परिभाषाओं को पेश किया गया है?
असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक: असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का क्या महत्व है?
D. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)
समेकित कानून: इसने किन 13 कानूनों को निरस्त किया है?
परिभाषाओं का विस्तार और प्रयोज्यता: इस संहिता में परिभाषाओं का विस्तार कैसे किया गया है और इसकी प्रयोज्यता कैसे बढ़ाई गई है?
महिला कर्मचारियों के अधिकार: महिला कर्मचारियों के संबंध में क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं?
अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक: अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या विशेष प्रावधान (जैसे यात्रा भत्ता) किए गए हैं?
दैनिक काम के घंटे: दैनिक काम के घंटे की सीमा क्या निर्धारित की गई है?
सलाहकार बोर्ड: राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड के गठन का क्या महत्व है?
ठेका श्रम पर प्रतिबंध: प्रतिष्ठानों की मुख्य गतिविधियों में ठेका श्रम के नियोजन पर प्रतिबंध का क्या निहितार्थ है?
ऑडियोविजुअल और बीड़ी-सिगार श्रमिक: ऑडियोविजुअल और बीड़ी-सिगार श्रमिकों के लिए क्या विशेष प्रावधान हैं?
VI. प्रभाव और भविष्य
“ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” पर प्रभाव: नए कोड भारत में “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” रैंकिंग में सुधार कैसे करेंगे?
दीर्घकालिक प्रभाव: इन कोड का अर्थव्यवस्था और संगठित और असंगठित श्रमिकों के कल्याण पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है?
कोर्स का ध्यान: इस कोर्स का मुख्य ध्यान क्या है (प्रयोज्यता, कार्यान्वयन, प्रभाव, कल्याणकारी उपाय)?
लाभार्थी: ये कोड किन वर्गों के लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं (श्रमिक, नियोक्ता, कर्मचारी, प्रबंधक)?
प्रश्नोत्तरी
1. भारत में नए श्रम कोडों को लागू करने के पीछे प्राथमिक प्रेरणा क्या है, विशेष रूप से ब्रिटिश-युग के कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने के संदर्भ में?
भारत में नए श्रम कोडों को लागू करने की प्राथमिक प्रेरणा पुरानी ब्रिटिश-युग की श्रम विधानों को पूरी तरह से निरस्त करना है, जिन्हें अप्रचलित माना जाता था। इसका उद्देश्य श्रम कानूनों के पूरे परिदृश्य को बदलना और भारत में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में सुधार करना है, जिससे आर्थिक विकास और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा मिले।
2. नए श्रम कोडों के तहत ‘सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमीकरण’ से आप क्या समझते हैं? यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को कैसे प्रभावित करेगा?
नए श्रम कोडों के तहत ‘सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमीकरण’ का अर्थ है कि सरकार का लक्ष्य देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। यह पहली बार है जब असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के समान लाभों के दायरे में लाया जाएगा।
3. वेतन संहिता, 2019 में ‘राष्ट्रीय फ्लोर वेज’ की अवधारणा क्यों पेश की गई है? इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को कैसे दूर करना है?
वेतन संहिता, 2019 में ‘राष्ट्रीय फ्लोर वेज’ की अवधारणा इसलिए पेश की गई है ताकि राज्यों के बीच न्यूनतम मजदूरी में मौजूदा क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी राज्य सरकार इस निर्धारित राष्ट्रीय फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी तय न कर सके, जिससे पूरे देश में मजदूरी के लिए एक समान आधार स्थापित हो सके।
4. गुजरात मजदूर सभा मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था? इसने महामारी के दौरान श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को कैसे प्रभावित किया?
गुजरात मजदूर सभा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि महामारी के दौरान लॉकडाउन का पूरा बोझ श्रमिकों पर नहीं डाला जाना चाहिए। न्यायालय ने संविधान के निर्देशक सिद्धांतों को बरकरार रखा, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा और कार्यस्थल में गरिमा और समानता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि श्रमिकों का शोषण न हो।
5. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ‘निश्चित अवधि रोजगार’ को वैध बनाती है। इस प्रावधान का क्या महत्व है और यह श्रमिकों को कौन से लाभ प्रदान करता है?
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में ‘निश्चित अवधि रोजगार’ को वैध बनाने का महत्व यह है कि यह इस प्रकार के रोजगार वाले श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों के समान सभी लाभ, जैसे कि उपहार, ईएसआई, पीएफ, और बोनस के लिए पात्र बनाता है। यह उद्योगों को लचीलापन प्रदान करता है जबकि यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण से समझौता न हो।
6. श्रम कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के संबंध में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का क्या महत्व है?
भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में ‘श्रम’ का महत्व यह है कि यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को श्रम से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि श्रम सुधारों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्देशित किया जा सकता है, जबकि राज्यों को विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कानूनों को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है।
7. ‘इंस्पेक्टर राज’ प्रणाली को समाप्त करने से क्या तात्पर्य है, और नए श्रम कोडों के तहत श्रम निरीक्षकों की भूमिका कैसे बदली है?
‘इंस्पेक्टर राज’ प्रणाली को समाप्त करने का अर्थ है श्रम निरीक्षकों की भूमिका को केवल नियामक से सुविधाकर्ता में बदलना। नए श्रम कोडों के तहत, उनकी भूमिका अब न केवल कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है, बल्कि नियोक्ताओं और श्रमिकों को नियमों का पालन करने में सहायता करना भी है, जिससे अधिक सहयोगात्मक और कम दंडात्मक वातावरण बन सके।
8. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए क्या नया प्रावधान पेश करती है?
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए एक ‘सामाजिक सुरक्षा निधि’ का प्रावधान पेश करती है। यह निधि विशेष रूप से इन अत्यधिक असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ और सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है, जो पहली बार उन्हें व्यापक सुरक्षा जाल के तहत लाती है।
9. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या विशिष्ट लाभ शामिल हैं?
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष लाभ शामिल हैं, जैसे पहली बार देश में यात्रा भत्ता का प्रावधान। यह संहिता उनकी कार्य स्थितियों, सुरक्षा और कल्याण को भी सुनिश्चित करती है, जिससे उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की अनुमति मिलती है।
10. नए श्रम कोड प्रधान मंत्री के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” और “आत्मनिर्भर भारत” के दृष्टिकोण के साथ कैसे संरेखित होते हैं?
नए श्रम कोड प्रधान मंत्री के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” और “आत्मनिर्भर भारत” के दृष्टिकोण के साथ संरेखित होते हैं, क्योंकि वे श्रम कानूनों को सरल बनाते हैं, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ाते हैं, और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। यह समेकन और सुधार भारत को एक आत्म-निर्भर राष्ट्र बनाने और सभी के लिए समावेशी विकास प्राप्त करने के बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं।
मुख्य शब्दों की शब्दावली
श्रम कोड (Labour Codes): भारत सरकार द्वारा पुराने श्रम कानूनों को समेकित करके बनाए गए चार नए कानून।
निरसन (Repeal): किसी मौजूदा कानून या नियम को औपचारिक रूप से रद्द करना या हटाना।
अधिसूचित (Notified): आधिकारिक तौर पर घोषित या सूचित किया गया, जिससे कोई कानून या प्रावधान कानूनी रूप से लागू हो जाता है।
श्रम सशक्तिकरण (Labour Empowerment): श्रमिकों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण में सुधार के लिए अधिक शक्ति और नियंत्रण प्रदान करना।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business): किसी देश में व्यवसाय स्थापित करने और संचालित करने की सुगमता का माप, जिसे अक्सर नियामक बाधाओं को कम करके मापा जाता है।
सामाजिक सुरक्षा (Social Security): स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन, बेरोजगारी लाभ, और अन्य कल्याणकारी उपायों के माध्यम से व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी योजनाएं।
संगठित क्षेत्र (Organized Sector): वे कार्यस्थल जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं, पंजीकृत होते हैं, और श्रमिकों को भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि जैसे लाभ प्राप्त होते हैं।
असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector): वे कार्यस्थल जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं, जहाँ रोजगार की शर्तें अनियमित होती हैं, और श्रमिकों को अक्सर संगठित क्षेत्र के समान लाभ नहीं मिलते।
ब्रिटिश-निर्मित कानून (British-Made Laws): औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में लागू किए गए कानून, जो स्वतंत्रता के बाद भी कई दशकों तक प्रभावी रहे।
श्रम कल्याण (Labour Welfare): श्रमिकों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और काम करने की स्थितियों में सुधार के लिए किए गए उपाय।
त्रिपक्षीय प्रणाली (Tripartite System): वह प्रणाली जहाँ नियोक्ता, कर्मचारी (ट्रेड यूनियन के माध्यम से), और सरकार श्रम संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एक साथ काम करते हैं।
ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926): एक कानून जिसने भारत में ट्रेड यूनियनों के गठन और उनके कार्यों को कानूनी मान्यता दी।
सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining): वह प्रक्रिया जिसमें कर्मचारी, एक ट्रेड यूनियन के माध्यम से, नियोक्ता के साथ मजदूरी, घंटे और अन्य रोजगार की शर्तों पर बातचीत करते हैं।
हायर एंड फायर (Hire and Fire): एक नीति जिसमें नियोक्ताओं को कर्मचारियों को आसानी से नियुक्त करने और बर्खास्त करने की अनुमति होती है, अक्सर न्यूनतम कानूनी बाधाओं के साथ।
आत्मनिर्भर (Atmanirbhar): आत्मनिर्भर या स्वावलंबी। प्रधानमंत्री के “आत्मनिर्भर भारत” के दृष्टिकोण से जुड़ा है।
फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948): एक कानून जो कारखानों में श्रमिकों की कार्य स्थितियों, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को नियंत्रित करता है।
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): भारतीय संविधान के भाग III में निहित मूलभूत मानवाधिकार जो सभी नागरिकों को प्राप्त हैं और राज्य के विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं।
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy – DPSP): भारतीय संविधान के भाग IV में निहित सिद्धांत जो सरकार को कानून और नीतियां बनाते समय मार्गदर्शन करते हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है।
समवर्ती सूची (Concurrent List): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में एक सूची जो उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं।
इंस्पेक्टर राज (Inspector Raj): एक नकारात्मक शब्द जिसका उपयोग उस प्रणाली का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहाँ सरकारी निरीक्षक (विशेषकर श्रम निरीक्षक) व्यवसायों को अत्यधिक विनियमित करते हैं, अक्सर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को बढ़ावा देते हैं।
वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019): चार पुराने कानूनों (जैसे भुगतान मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम) को समेकित करने वाला पहला नया श्रम कोड।
राष्ट्रीय फ्लोर वेज (National Floor Wage): केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की एक आधार दर जिसके नीचे कोई भी राज्य न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकता।
गुजरात मजदूर सभा और अन्य बनाम गुजरात राज्य (Gujarat Mazdoor Sabha and Others vs. State of Gujarat): महामारी के दौरान श्रमिकों के कल्याण से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन किया।
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020): औद्योगिक विवादों के निपटारे, ट्रेड यूनियनों और स्थायी आदेशों से संबंधित तीन पुराने कानूनों को समेकित करने वाला कोड।
निश्चित अवधि रोजगार (Fixed Term Employment): एक विशिष्ट अवधि के लिए रोजगार का अनुबंध, जो स्थायी रोजगार से भिन्न होता है लेकिन नए कोड के तहत समान लाभ प्रदान करता है।
एकल वार्ताकार ट्रेड यूनियन (Single Negotiating Trade Union): एक उद्योग में केवल एक ट्रेड यूनियन को मान्यता देना जो प्रबंधन के साथ सामूहिक सौदेबाजी कर सके, ताकि विवादों को कम किया जा सके।
शिकायत निवारण समितियां (Grievance Redressal Committees): कार्यस्थल पर कर्मचारियों की शिकायतों को हल करने के लिए गठित समितियां।
स्थायी आदेश (Standing Orders): एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों का एक सेट।
ग्रेच्युटी (Gratuity): एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला एकमुश्त भुगतान, आमतौर पर सेवा की एक निश्चित संख्या पूरी करने पर।
कर्मचारी राज्य बीमा (Employee State Insurance – ESI): कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित लाभ प्रदान करने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना।
कर्मचारी भविष्य निधि (Employees’ Provident Fund – EPF): सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली एक बचत योजना।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code, 2020): सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ मौजूदा कानूनों को समेकित करने वाला कोड।
गिग श्रमिक (Gig Workers): वे व्यक्ति जो अल्पकालिक अनुबंधों या स्वतंत्र कार्य के माध्यम से आय अर्जित करते हैं, अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
प्लेटफॉर्म श्रमिक (Platform Workers): वे व्यक्ति जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे राइड-शेयरिंग या खाद्य वितरण।
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020): कार्यस्थल में सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिकों की कार्य स्थितियों से संबंधित 13 कानूनों को निरस्त करने वाला कोड।
अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक (Inter-State Migrant Workers): वे श्रमिक जो रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं।
ठेका श्रम (Contract Labour): एक ठेकेदार के माध्यम से नियोजित श्रमिक, जो सीधे नियोक्ता द्वारा नियोजित नहीं होते हैं।
¿Para quién es este curso?
- Labour Laws Students
- Labour Laws practitioner
- HR Professionals
- Law Professional
- Business owners
- Employees/ Worker
- Contractors
- Union / Union Members
- Investors
Ver másVer menos
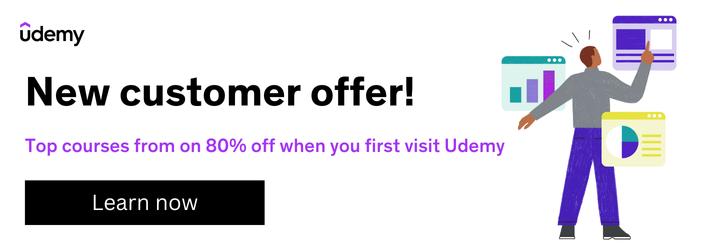





Reviews
There are no reviews yet.